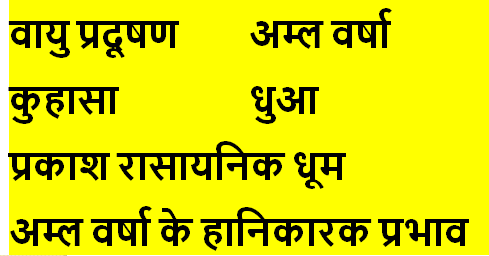वायुमण्डलीय प्रदूषण में कणिकाएँ
हम देखते हैं कि डीजल ट्रक द्वारा वायुमण्डल में छोड़ा गया काला धुंआ प्रदूषण का सर्वाधिक स्पष्ट रूप है। धुंए में कणिकीय पदार्थ होते हैं। कणिकाएं लघु ठोस अथवा द्रवीय कण होते हैं जो वायु में निलम्बित रहते हैं।
यद्यपि आंख द्वारा कणिकाओं को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता ये कणिकाएं सम्मिलित होकर धुंध बनाती है जिसके कारण देखने में अवरोध उत्पन्न होता है। वायुमण्डल में कणिकाऐ जीवनक्षम अथवा अजीवनक्षम दोनों ही प्रकार की हो सकती है।
जीवनक्षम कणिकाएं सूक्ष्म जीव है जो वायुमण्डल में परिक्षिप्त होती है। इनमें जीवाणु, कवक, फफूंद तथा शैवाल आदि सम्मिलित हैं | इसके अतिरिक्त कवक पौधों में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। प्रमुख अजीवनक्षम कणिकाएं या तो वहद पदार्थ के विखंडन के फलस्वरूप बनती है अथवा सूक्ष्म कणों या सूक्ष्म-बूंदों के संघनन, निर्मित होती है। वायुमण्डल में चार प्रकार की अजीवनक्षम कणिकाएँ उपस्थित रहती है : कहासा, धुंआ, धूम, धूल।
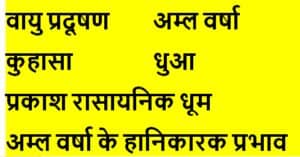
कुहासा : यह स्प्रे द्रव के कणों तथा वायु में उपस्थित दाष्पों के संघनन से बनता है| उदाहरणार्थ – शाकनाशियों तथा कीटनाशियों की अवशिष्ट मात्राएं वायु में फैलकर कुहासा बनाती है।
धुआ : कार्बनिक पदार्थ के दहन तथा जलाने के फलस्वरूप उत्पन्न काजल के सूक्ष्म कण धुंआ निर्मित करते हैं। तेल धुंआ, तंबाकू धुंआ तथा कार्बन धुंआ इस प्रकार के कणकीय उत्सर्जन के कुछ उदाहरण है|
धूम एवं संघनित वाष्प : धातुओं के धूम इस वर्ग के भलीभांति ज्ञात कणिकाएं है | इस वर्ग में धातुकर्मीय धूम तथा क्षार धूम भी आते हैं।
धूल : ये महीन कण हैं जो ठोस पदार्थ के कूटनें, पीसने तथा प्रयुक्त करने के समय उत्पन्न होते हैं। पिसा चूने का पत्थर, प्लवन के फलस्वरूप उड़ा बालू, पीसा हुआ कोयला, सीमेंट, फ्लाइ ऐश तथा सिलिका धूल वायुमण्डल में उपस्थित अजीवनक्षमी धूल कणिकाओं के कुछ उदाहरण हैं|
कणिकीय प्रदूषकों का प्रभाव साधारणतः कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। 5 माइक्रोन से बड़े आकार के कण साधारणत: नाक के छिद्र में रूक जाते हैं परंतु इससे बारीक कण फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। फेफड़ों में घुसने की गति कणिकाओं के आकार के विलोमानुपाती होती है। इन बारीक कणिकाओं में से अनेक कैंसरकारक होती है। बारीक कणों के अन्तःश्वसन के कारण फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न होता है। लम्बे समय तक ऐसे वातावरण में रहने पर फेफड़ों की सतह पर “क्षतचिन्हता” अथवा “फाइब्रोसिस” हो जाती है।
उद्योगों में कार्य करने वाले वालों में यह एक सामान्य रोग है जिसको “न्यूमोकोनिओसिस” कहते हैं। वायुमण्डल में निलंबित कणिकीय पदार्थ पथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों को प्रभावी ढंग से रोकता है। जिसके कारण पथ्वी का ताप कम हो जाता है। वे सूर्य के प्रकाश को पथ्वी तक पहुंचने से रोककर पथ्वी का ताप कम करते हैं और वे शहरों में कोहरे और बारिश को बढ़ाने में योगदान देते हैं। शहर के वायुमण्डल में निलंबित कणों की उपस्थिति के कारण दश्यता भी कम हो जाती है। वायुमण्डल में जैसे-जैसे कणिकीय सान्द्रता बढ़ती है, वैसे-वैसे दश्यता घटती है|
वायु प्रदूषण के कुछ प्रभाव-
१. धूम कोहरा
धुंआ तथा कोहरा का सम्मिलित रूप धूम-कोहरा कहलाता है। विश्व के अनेक शहरों में सर्वविदित वायु प्रदूषण धूम-कीहरा के कारण हैं। धूम-कोहरा दो प्रकार का होता है :
(अ ) सामान्य धूम-कोहरा जो ठंडी, नम जलवायु में होता है। इसका कारण ईंधन दहन के फलस्वरूप वायुमण्डल में सल्फर के ऑक्साइडों तथा कणिकीय पदार्थ की सान्द्रता बढ़ना है तथा
(ब) प्रकाश रासायनिक धूम-
कोहरा जो उष्ण, शुष्क तथा साफ सूर्यमयी जलवायु में होता है। यह स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम-कोहरा की रासायनिक प्रकृति ऑक्सीकारक है क्योंकि इसमें ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की उच्च सान्द्रता रहती है जबकि प्रतिष्ठित धूम-कोहरा अपचायक होता है क्योंकि उसमें 50, की उच्च सान्द्रता होती है। प्रकाश रासायनिक धूम-कोहरा सामान्यतः उच्च जनसंख्या के शहरों में होता है जिनमे मोटर वाहनों की सघनता अधिक होती है।
(a ) प्रकाश रासायनिक धूम-कोहरा का निर्माण :
प्रकाश रासायनिक धूम-कोहरा के निर्माण की रासायनिक प्रक्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड (0४0) पर केन्द्रित है। कारों तथा ट्रकों के पेट्रोल व डीजल इंजनों में उच्च ताप पर , तथा 0, अभिक्रिया कर 1३0 की कुछ मात्रा बनाते हैं जो वायु में अन्य गैसों के साथ उत्सर्जित होती है। वायु में 10,190, में ऑक्सीकृत होती है जो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड तथा मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में विघटित हो जाती है (प्रकाश रासायनिक विघटन) :
NO2 ⟶ NO + O
ऑक्सीजन परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण o, के साथ संयुक्त होकर ओजोन में परिवर्तित हो सकता है
O2 + O ⟶ O3
उपुर्यक्त अभिक्रिया में निर्मित O, शीघ्रतापूर्वक अभिक्रिया में उत्पन्न NO के साथ अभिक्रिया कर पुनः NO2, बनाती है :
O3 + NO ⟶ NO2 + O2
NO2 तथाO2 दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण, प्रदूषित वायु में उपस्थित अदहित हाइड्रोकार्बनों के साथ अभिक्रिया कर कई रसायनों, जैसे, फार्मल्डिहाइड, ऐक्रोलीन तथा परॉक्सीऐसीटिल नाइट्रेट (PAN) का निर्माण करते हैं जो आंखों में जलन पैदा कर आंसू लाते हैं तथा श्वसन तंत्र के लिए भी हानिकारक हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कृहरे का भूरा धुंध NO2 के भूरे रंग के कारण होता है।
CH4 + 2O3 ⟶ 3CH2=O + 2H2O
फार्मेल्डिहाइड
ऐक्रोलीन तथा परॉक्सीऐसीटिल नाइट्रेट ((PAN) विशेष रूप से हानिकारक है।
प्रकाश रासायनिक धूम-कोहरे के प्रभाव:
प्रकाश रासायनिक धूम-कोहरे के तीन मुख्य घटक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा कार्बनिक ब्युत्पन्न (जैसे, एक्रोलीन, फार्मेल्डिहाइड, पीएएन, आदि) है। इन सभी पदार्थों के कारण धूम कुहरा हानिकारक है। प्रकाश रासायनिक घूम-कोहरे के कारण खांसी, सांस में घरघराहट, श्वासनली में संकचन तथा श्वसन श्लेष्मल झिल्ली का प्रदाह आदि रोग उत्पन्न होते हैं। धूम-कोहरे में उपस्थित परॉक्सीऐसीटिल नाइट्रेट तथा ऐल्डिहाइड आंखों में प्रदाह उत्पन्न करते हैं।
धूम-कोहरे के कुछ घटक कृछ पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं रबड़ ओजोन के साथ अभिक्रिया करती है जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं और वह शीघ्र ही खंडित होकर नष्ट हो जाती है। धूम-कोहरे का पौधों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ओजोन वनस्पति को नष्ट करती है, पौधों की वद्धि को रोकती है तथा फसल के उत्पादन को भी कम करती है। धूम-कोहरे के सभी घटकों में से पीएएन का पौधों पर सर्वाधिक विषाक्त प्रभाव पडता है। यह नई पत्तियों पर आक्रमण कर उनकी सतह का कांस्यन तथा काचितीकरण करती है।
प्रकाश रासायनिक धूम-कोहरे पर नियंत्रण :
इसको कम करने तथा उसके निर्माण को रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। स्वचालित वाहनों में अच्छी किस्म के उत्प्रेरित परिवर्तक लगाकर धूम-कोहरे का निर्माण कम किया जा सकता है क्योंकि यह वायुमण्डल में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बनों के उत्सर्जन को रोकता है। कुछ पदार्थोंए॥के उपयोग द्वारा भी प्रकाश रासायनिक धूम-कुहरा कम किया जा सकता है।
ये पदार्थ मुक्त मूलक ट्रैप विपाशक के रूप में कार्य करते हैं| अर्थात् इन पदार्थों को वायुमण्डल में छिड़कने पर वे मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं जो प्रकाश रासायनिक धूम-कहरे के मुक्त मूलकीय पूर्ववर्तियों के साथ शीघ्रतापूर्वक संयुक्त होकर उन्हें नष्ट कर देते हैं।
(॥) अम्ल वर्षा
जब वर्षा में H2SO4 , HNO3,(अल्प मात्रा में HCl) मिले हो तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ये अम्ल S एवं N2, के ऑक्साइड से बनते हैं। अम्ल वर्षा की pH 4-5 होती है।
(A) अम्ल वर्षा का निर्माण :
N के ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। बाद में वातावरण में उपस्थित जल वाष्प से क्रिया कर HNO3, बनता है।
पद; 1 NO + O3 ⟶ NO2 + O2
NO2 + O3 ⟶ NO3 + O2
NO2 + NO3 ⟶ N2O5
N2O5 + H2O ⟶ 2HNO3
वर्षा के साथ पथ्वी पर HNO3आता है।
पद 2: 2SO2 + O2 ⟶ 2SO3
SO3 जल वाष् से क्रिया कर H2SO4 बनाती है।
pH मान | बफर विलयन | ले शातेलिए का नियम | BEST NOTES 11TH CLASS
HNO3 एवं H2SO4 वायु में उपस्थित HCl के साथ मिलकर अम्लीय अवक्षेप बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं।
अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव –
- यह बिल्डिंग एवं मूर्तियां जो मार्बल या चूने के पत्थर या मोर्टर से बनी हो, उनको नुकसान पहुंचाती है